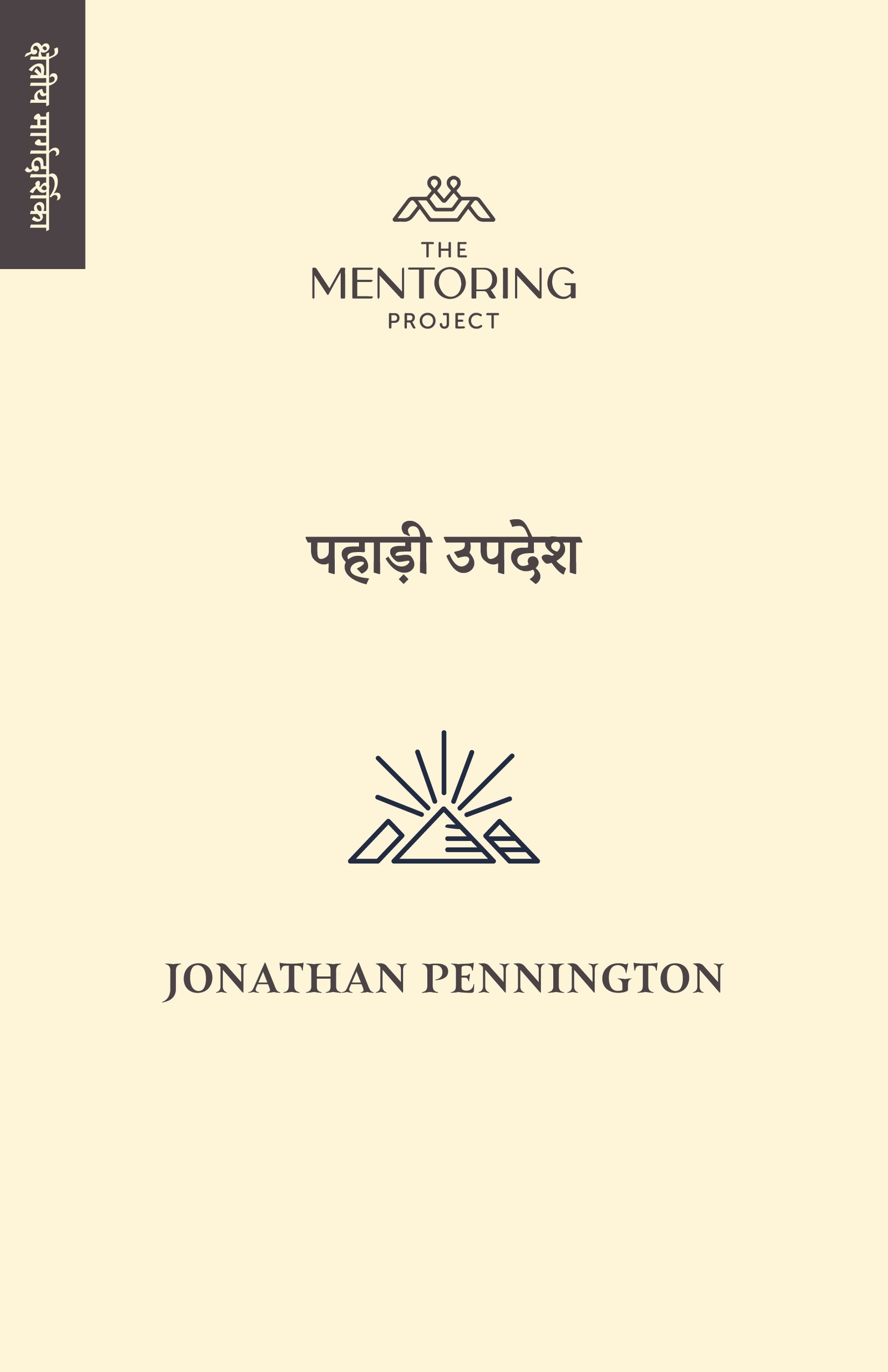
#17 पहाड़ी उपदेश
परिचय
यीशु का जूआ — मार्गदर्शन जीवन देने वाले के रूप में मसीहियत
पिछले दो हज़ार वर्षों में, क्रूस एक ऐसा चिन्ह रहा है जो मसीही कला, ईश्वर विज्ञान, आभूषण, वास्तुकला, झण्डों और यहाँ तक कि त्वचा में कलाकृति गोदने तक का मुख्य केंद्र रहा है। मसीही समाज में सभी छवियों और मूर्तियों में यीशु के क्रूस को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अनगिनत उपदेश और पुस्तकें क्रूस के महत्व के विषय में बताती हैं। कलीसियाओं और सेवकाईयों के नाम में प्रायः “क्रूस” सम्मिलित होती है। और हाल के समय में अधिकाँश कलीसियाओं के भवन क्रूस के आकार में बनाए जाते थे, जिनमें वेदी बीच केन्द्र में होती थी।
इस क्रूस का बीच में आना समझ में आता है, क्योंकि यीशु ने स्वेच्छा से क्रूस पर बलिदान दिया है (मत्ती 26:33-50)। यीशु ने अपने शिष्यों से बार-बार कहा कि उन्हें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना चाहिए (मत्ती 10:38; 16:24; मरकुस 8:34; लूका 14:27)। प्रेरित पौलुस ने मसीही जीवन के विषय में अधिकाँश बातें इस प्रकार से कही कि यह मसीह के क्रूस को, उसके दर्द को, और उसकी लज्जा को अपनाने का जीवन है (1 कुरिन्थियों 1:17–28; गलातियों 6:14; कुलुस्सियों 1:19–23)।
फिर भी, एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसका प्रयोग यीशु ने किया, जो मसीही विचारधारा में क्रूस के जितना प्रमुख नहीं रहा, परन्तु मेरा मानना है कि उसे होना चाहिए: और वह यीशु का जूआ है। मत्ती रचित सुसमाचार का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि यद्यपि यह केवल एक ही पाठ में पाया जाता है, फिर भी जूआ मत्ती रचित सुसमाचार के ईश्वर विज्ञान और उद्देश्य तथा यीशु की सम्पूर्ण सेवकाई का मुख्य केन्द्र रहा है। मत्ती 11:28–30 में, परमेश्वर को प्रकट करने वाले के रूप में अपनी अनोखी भूमिका का साहसपूर्वक दावा करने (11:25–27) के पश्चात्, यीशु लोगों को अपने जीवन में उसका जूआ उठाने के लिए आमंत्रित करता है।
हे सब परिश्रम करनेवालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो; और मुझसे सीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ: और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। (मत्ती 11:28-30)
जूआ और क्रूस दोनों ही लकड़ी के बने होते हैं, परन्तु जूआ फाँसी का प्रतीक न होकर एक कृषि सम्बन्धी यंत्र होता है। जूआ एक किसान को धैर्यपूर्वक एक पशु को खेत की लम्बी कतार में ले जाते हुए, तथा बैल या गाय को दिशा-निर्देश देते हुए चित्रित करता है, क्योंकि वह भूमि को जोतता है और बुवाई के लिए खेत तैयार करता है।
यीशु ने अपने जुए को हमारी गर्दन पर रखने के निमंत्रण का अर्थ शीघ्र ही स्पष्ट कर दिया —जिसका अर्थ है कि “मुझसे सीखो” (मत्ती 11:29)। यहाँ “सीखना” शब्द का अनुवाद “शिष्य बनना” के लिए किया गया है, अर्थात्, एक ऐसा व्यक्ति जो एक कुशल शिक्षक का छात्र बनता है, जो एक विशेषज्ञ के वचनों तथा उदाहरण से सीखता है। और जहाँ क्रूस आत्म-बलिदान की बात करता है, वहीं जुआ शिष्यत्व या मार्गदर्शन की बात करता है। यही मसीहियत है: यीशु का निमंत्रण है कि हम उससे सच्ची शान्ति पाने का तरीका सीखें, और वह बहुतायत का जीवन भी पाएँ जिसके लिए हम बनाए गए हैं और जिसकी हम लालसा भी करते हैं। यीशु कह रहा है कि ऐसा सच्चा विश्राम केवल तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में उसका जूआ उठाएँगे और उसके शिष्य बनेंगे तथा उसे अपना सच्चा मार्गदर्शक मानकर उसके अधीन हो जाएँगे।
ऑडियो मार्गदर्शिका
ऑडियो#17 पहाड़ी उपदेश
1
मत्ती रचित सुसमाचार शिष्य बनाने वाली पुस्तक के रूप में है
यीशु को एक गुरु, शिष्य बनाने वाला और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करने वाली छवि सभी सुसमाचारों में मिलती है, परन्तु सबसे स्पष्ट रूप से यह मत्ती रचित सुसमाचार में मिलती है। आरम्भ से अन्त तक मत्ती का सुसमाचार शिष्यत्व के विषय में बोलता है, और पूरी कहानी एक शिष्य-निर्माण करने वाली पुस्तक के रूप में व्यवस्थित की गई है।
जब यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला प्रचार करने के लिए आता है, तो उसका सन्देश स्वर्ग के राज्य के आगमन के कारण, पश्चाताप करने के लिए एक बुलावा होता है (3:2)। और यीशु ने भी अपनी सेवकाई आरम्भ करते समय ठीक यही बात कही थी (4:17)। पश्चाताप करने के लिए बुलाया जाना निन्दा का सन्देश नहीं है, वरन् आमन्त्रित करने का सन्देश है। पश्चाताप करने के लिए बुलाया जाना बहुत अधिक अपराधी होने का सन्देश नहीं है, वरन् संसार को देखने और जीने के तरीके से मुड़कर परमेश्वर के जीवन के तरीके की ओर लौटने की बुलाहट है। पश्चाताप शिष्यत्व की भाषा है।
मत्ती की प्रसिद्ध कहानी के अन्तिम निष्कर्ष में भी शिष्यत्व पर ही बल दिया गया है। अपनी “बड़ी आज्ञा” (मत्ती 28:16–20) में, यीशु अपने शिष्यों को अपने ही अधिकार के साथ भेजता है ताकि वे हर जाति के लोगों को “शिष्य” बनाएँ। यह शिष्यत्व जीवन से जीवन तक का मार्गदर्शन है, जो त्रिएक परमेश्वर (पिता, पुत्र और आत्मा के नाम में) में पाया जाता है, और यह लोगों को बपतिस्मा और शिक्षा देने के रूप में उपयोग किया जाता है। बपतिस्मा देना लोगों को यीशु के साथ अपनी पहचान बनाने तथा उसके अन्य शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण है। शिक्षा देना एक ऐसा निमंत्रण है जिसमें लोग यीशु की शिक्षाओं के अनुसार सिद्धान्त, नैतिकता, प्रवृत्ति और संवेदनशीलता—जिनका नमूना स्वयं यीशु ने प्रस्तुत किया, उनके आधार पर संसार में जीना सीखते हैं। यही मार्गदर्शन है, और मसीहियत में इससे बढ़कर कोई और बात नहीं है।
परन्तु शिष्यत्व के महत्व पर ऐसा बल केवल मत्ती के सुसमाचार के आरम्भ और अन्त में ही नहीं है। पश्चाताप करने के लिए आरम्भिक बुलाहट और “जाकर शिष्य बनाने” की अन्तिम आज्ञा के बीच, सम्पूर्ण मत्ती रचित सुसमाचार शिष्य निर्माण के दर्शन पर आधारित है। मत्ती ने अपने सुसमाचार के मुख्य भाग को पाँच बड़े शिक्षा के खण्डों के आस-पास व्यवस्थित करके इस बात को प्रकट किया है (अध्याय 5-7, 10, 13, 18, 23-25)। ये खण्ड यीशु की शिक्षाओं का संग्रह हैं, जिनका उद्देश्य शिष्यत्व है।
प्राचीन संसार में प्रसिद्ध शिक्षकों और दार्शनिकों के विषय में बहुत सी जीवनी लिखी गई थीं। शिक्षक की बातों को अधिकाँश एक विषय पर आधारित स्मरणीय संकलनों में एकत्रित किया जाता था, जिन्हें “प्रतीक” कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति जीवन या धर्म का कोई विशेष दर्शनशास्त्र सीखना चाहता था, तो प्रतीक उन्हें वास्तविक जीवन में ध्यान और अभ्यास करने के लिए निर्देशों का एक सरल, संग्रह प्रदान करता था। ये प्रतीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि प्राचीन संसार में बहुत कम लोगों के पास शिक्षा की पहुँच थी, तथा अधिकाँश लोग मूलभूत संकेतों से पढ़ या लिख नहीं सकते थे। इसलिए किसी विषय पर आधारित शिक्षाओं का स्मरणीय खण्ड होना मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता था।
इसलिए मत्ती, जो स्वयं यीशु का शिष्य है प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए और अधिक शिष्य बनाने के लिए समर्पित हैं, उसने यीशु के गुरु होने के विषय में एक उत्कृष्ट जीवनी इसी उद्देश्य से लिखी। और वह लोगों को पश्चाताप करने और यीशु का जूआ अपने ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे जीवन पाएँ। संक्षेप में, मत्ती हमें मसीही राज्य के शिष्यत्व के मार्ग पर मार्गदर्शन पाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यीशु ने जो कार्य किए उसकी कहानियाँ और उसकी शिक्षाओं के संग्रह इस उद्देश्य के लिए अत्यंत आवश्यक थे।
मत्ती रचित सुसमाचार इस प्रकार से व्यवस्थित है, जिसमें पाँच शिक्षा के खण्डों पर प्रकाश डाला गया है:
- उत्पत्ति और आरम्भ (1:1–4:22)
- परिचय (1:1–4:16)
- सेतु (मत्ती 4:17–22)
- प्रकाशन और विभाजन: वचन और कार्य में (मत्ती 4:23–9:38)
- पहल प्रतीक (5:1–7:29)
- पहला वृत्तांत (8:1–9:38)
- प्रकाशन और विभाजन: जैसा गुरु, वैसे ही शिष्य (मत्ती 10:1–12:50)
- दूसरा प्रतीक (10:1–11:1)
- दूसरा वृतांत (11:2–12:50)
- प्रकाशन और विभाजन: एक नई, अलग ठहराई गई परमेश्वर की प्रजा (मत्ती 13:1–17:27)
- तीसरा प्रतीक (13:1–53)
- तीसरा वृतांत (13:54–17:27)
- प्रकाशन और विभाजन: नए समुदाय के भीतर और बाहर (मत्ती 18:1–20:34)
- चौथा प्रतीक (18:1–19:1)
- चौथा वृतांत (19:2–20:34)
- प्रकाशन और विभाजन: न्याय — अभी और भविष्य में (मत्ती 21:1–25:46)
- पाँचवाँ वृतांत (21:1–22:46)
- पाँचवाँ प्रतीक (23:1–25:46)
- अन्त और आरम्भ (मत्ती 26:1–28:20)
- सेतु (मत्ती 26:1–16)
- निष्कर्ष (मत्ती 26:17–28:20)
इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि सम्पूर्ण सुसमाचार शिष्य-निर्माण के लिए समर्पित है और ये पाँच प्रतीक मार्गदर्शन सामग्री की उच्चतम एकाग्रता प्रदान करते हैं।
प्रसिद्ध उपदेश पर ध्यान देना: पहाड़ी उपदेश
कलीसिया के इतिहास में, इस आदर्श उदाहरण से पहले — मत्ती 5–7 — सम्पूर्ण बाइबल का सबसे प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रचारित, अध्ययन किया गया, लिखा गया और प्रसिद्ध भाग रहा है। और अगस्टीन के दिनों से ही इन अध्यायों को “पहाड़ी उपदेश” का शीर्षक दिया गया है।
विभिन्न संप्रदायों और ईश्वर विज्ञान की परम्पराओं के बीच मतभेदों का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वे इन मौलिक अध्यायों की किस प्रकार से भिन्न-भिन्न व्याख्या करते हैं। मैं अधिकतर पहाड़ी उपदेश का वर्णन एक तरणताल (स्विमिंग पूल) के पानी का परिक्षण करने वाले यंत्र के समान करता हूँ, जो क्लोरीन स्तर, पी.एच. सन्तुलन और क्षारीयता को दर्शाता है। यदि हम किसी भी ईश्वर विज्ञानी या सम्प्रदाय को पहाड़ी उपदेश में डुबो दें, तो यह तुरन्त ही हमें उनके ईश्वर विज्ञान, समझ तथा समर्पण के विषय में बहुत कुछ बता देगा। क्योंकि पहाड़ी उपदेश कई महत्वपूर्ण सत्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे — पुराना नियम और यीशु की शिक्षाओं का आपसी सम्बन्ध, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होने का अर्थ क्या है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और धन से हमारा किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए।
पहाड़ी उपदेश हमें वह सब कुछ नहीं देता जो हमें यीशु के विश्वासयोग्य शिष्य बनने के लिए जानना आवश्यक है। यह मत्ती रचित सुसमाचार में पाँच शिक्षण खण्डों में से केवल एक है; यह मत्ती की अन्य शिक्षाओं का भी हिस्सा है, और हमारे पास शेष सम्पूर्ण बाइबल भी है! परन्तु यह उपदेश एक कारण से प्रसिद्ध है: यह शिष्यत्व के जीवन के लिए विस्तृत, गहन और आधारभूत है। ये तीन अध्याय यीशु का जूआ अपने ऊपर उठाने, और जो राजाओं के राजा और देहधारी परमेश्वर की बुद्धि है, उससे मार्गदर्शन पाने तथा सीखने के लिए उत्तम स्थान हैं।
यीशु अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश का समापन दो लोगों की छवि के साथ करता है जो अपने घर को अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं (मत्ती 7:24-27) — उनमें से एक मूर्ख व्यक्ति है और दूसरा बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति यीशु की शिक्षाएँ सुनता तो है, परन्तु उनका पालन नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर, बुद्धिमान व्यक्ति यीशु के वचनों को सुनता है और उन पर चलता भी है। इस उपदेश में यह अन्तिम छवि इसलिए है क्योंकि मत्ती 5–7 का पूरा सन्देश बुद्धि के लिए निमंत्रण देता है। बुद्धि को संसार में रहने के लिए ऐसे अभ्यास करने के तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है जो परमेश्वर के राज्य के अनुरूप हो और जिनका परिणाम वह सच्ची मानवीय उन्नति हो जिसकी हम अभिलाषा करते हैं। यही वह शिष्यत्व है जिसके लिए यीशु हमें आमंत्रित करता है। और यदि हम उससे मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार हैं तो यही वह जूआ है जो वह हमें दे रहा है।
जिस प्रकार से सम्पूर्ण मत्ती रचित सुसमाचार उद्देश्यपूर्ण रचा गया है, उसी प्रकार पहाड़ी उपदेश भी है। यह उपदेश यीशु के कथनों का कोई उत्तम संग्रह नहीं है, वरन् अत्यधिक सुनियोजित ढँग से और सुन्दरता के साथ रचा गया सन्देश है। यीशु का उपदेश इस प्रकार व्यवस्थित है:
- परिचय: परमेश्वर के लोगों के लिए बुलावा (5:3–16)
- परमेश्वर के नए लोगों के लिए नौ धन्य वचन (5:3–12)
- परमेश्वर के लोगों की नई वाचा की साक्षी (5:13–16)
- मुख्य विषय: परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी धार्मिकता (ब.धा.) (5:17–7:12)
- परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के सम्बन्ध में बड़ी धार्मिकता (5:17–48)
- प्रस्ताव (5:17–20)
- छह व्याख्याएँ/उदाहरण (5:21–47)
- साराँश (5:48)
- परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति में बड़ी धार्मिकता (6:1–21)
- परिचय: मनुष्यों को नहीं, परन्तु स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना (6:1)
- तीन उदाहरण (6:2–18)
- परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के सम्बन्ध में बड़ी धार्मिकता (5:17–48)
**प्रार्थना पर विस्तृत चर्चा (6:7–15)
- निष्कर्ष: पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में प्रतिफल (6:19–21)
- संसार के साथ हमारे सम्बन्धों में बड़ी धार्मिकता (6:19–7:12)
- परिचय (6:19–21)
- इस संसार की वस्तुओं के सम्बन्ध में (6:22–34)
- इस संसार के लोगों के सम्बन्ध में (7:1–6)
- निष्कर्ष (7:7–12)
- संसार के साथ हमारे सम्बन्धों में बड़ी धार्मिकता (6:19–7:12)
- निष्कर्ष: भविष्य के प्रकाश में बुद्धि का निमंत्रण (7:13–27)
- दो प्रकार के मार्ग (7:13–14)
- दो प्रकार के भविष्यद्वक्ता (7:15–23)
- दो प्रकार के निर्माता (7:24–27)
हम देख सकते हैं कि उपदेश एक उत्तम नमूने के दर्शाता है —जैसे कि परिचय, मुख्य विषय, और निष्कर्ष। सम्पूर्ण सन्देश में प्रत्येक भाग की अपनी भूमिका है। यह सन्देश बुद्धि, शान्ति, और बहुतायत के जीवन के लिए निमंत्रण देता है जो यीशु के जूए को अपने ऊपर उठाने से प्राप्त होता है।
इससे आगे हम यीशु के उपदेश के प्रत्येक भाग पर ध्यान देंगे और उसके द्वारा सिखाई गई बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ यीशु की शिक्षाओं के विषय में सब कुछ तो नहीं कह पाएँगे,1 परन्तु हम कुछ खण्डों को आपस में जोड़ेंगे और सामान्य रूपरेखा का पालन करते हुए यह प्रश्न पूछेंगे कि, “यीशु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना कैसा लगता है?”
चर्चा एवं मनन:
- आप किन-किन तरीक़ों से इस प्रलोभन में पड़ते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं, वरन् संसार के अनुसार जीवन बिताएँ?
- आप अपने जीवन के किन क्षेत्रों में अधिक उन्नति देखना चाहते हैं?
2
आनन्द के विषय में हमारी धारणाओं को नया रूप देना (5:3–16)
एक पास्टर होने के नाते, मैं लोगों से नियमित रूप से एक प्रश्न पूछता हूँ कि, “जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको अच्छा जीवन पाने के विषय में कौन सा सन्देश मिला था?”
यह अपने आप से पूछने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सभी को किसी न किसी प्रकार का सन्देश मिला है, और वह सन्देश हमारे जीवन को अच्छे या बुरे रूप से प्रभावित करता रहा है, चाहे हमें इसका अनुभव हो या न हो।
जिन-जिन लोगों से मैंने यह प्रश्न पूछा है, वे सभी कोई न कोई उत्तर लेकर सामने आते हैं। बहुत से लोग तुरन्त ही एक छोटा सी बात कहते हैं, जो माता-पिता, चाचा या मार्गदर्शक ने उन्हें बार-बार कही थी। जैसे कि:
- “यदि दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग अपने साथियों की तुलना में अधिक परिश्रम करते हैं, तो भी उनका कार्य अधिक आनन्द दायक होगा, इसलिए, उन्हें परिश्रम जैसा कुछ अनुभव नहीं होगा।”
- “कठिन परिश्रम करो। अच्छे अंक प्राप्त करो। एक अच्छा जीवनसाथी ढूँढो।”
- “परमेश्वर से प्रेम करो। और दूसरों से भी प्रेम करो।”
- “शोकसभा में बोले जाने वाले शब्दों को ध्यान में रखकर जीवन जियो।”
- “इस बात की चिन्ता मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं। केवल स्वयं में ही बने रहें।”
या, यदि अन्तरिक्ष युद्ध (स्टार वार्स) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो आप यह सुन सकते हैं:
- मास्टर योदा कहते हैं कि, “करो या मत करो, प्रयास करने जैसा कुछ नहीं है।”
हम इन छोटे और महत्वपूर्ण कथनों को “सूत्र” कहते हैं। और यह सुन्दर कथन जीवन की अनगिनत अप्रत्याशित परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बुद्धिमानी से परिपूर्ण वचन होते हैं। प्राचीन संसार में, आत्मिक या दार्शनिक मार्गदर्शक एक प्रकार की कहावत का प्रयोग करते थे जिसे मैकरिज्म कहते हैं, यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ सच में आनन्दित होना या फलना-फूलना (मकारियोस) है। मैकरिज्म एक ऐसा कथन है जो एक अच्छे और सुन्दर जीवन जीने के तरीके का वर्णन करता है। मैकरिज्म एक निश्चित मानसिकता और आदतों को अपनाने का निमंत्रण देता है ताकि हम सच्ची मानवीय समृद्धि पा सकें।
मैकरिज्म का उपयोग सामान्यतः इसके विपरीत शब्दों के साथ किया जाता था: जैसे संकट। संकट को श्राप नहीं समझा जाता था। ये चेतावनी है कि संसार में कुछ तरीके से जीवन जीने पर हानि और दुःख होगा। इसी प्रकार, मैकरिज़्म भी कोई आशीर्वाद नहीं हैं। ये अच्छे जीवन के लिए निमंत्रण हैं। जब इन्हें मिलाकर देखा जाता है, तो मैकरिज्म और दुःख को अधिकाँश जीवन के दो तरीके या दो मार्ग के रूप में वर्णित किए जाते हैं, जो भिन्न-भिन्न दिशा में जाते हैं और बहुत विभिन्न अनुभवों के साथ समाप्त होते हैं।
मैकरिज्म और संकट का यह संयोजन सम्पूर्ण बाइबल में पाया जाता है, जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि के लिए निमंत्रण है, जो जीवन के मार्ग के बीच विनाश और अन्तर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, नीतिवचन की सम्पूर्ण पुस्तक ऐसे वचनों से भरी हुई है, विशेष रूप से आरम्भ के नौ अध्याय, जो दो मार्गों के विचार पर आधारित हैं। राजा सुलैमान ने अपने पुत्र के लिए जीवन जीने के दो भिन्न-भिन्न मार्गों का चित्रण किया है; एक मार्ग वह है जो जीवन लाएगा और दूसरा विनाश लेकर आएगा। इसी प्रकार, भजन संहिता 1, जिसे सामान्यतः बुद्धि का भजन कहा जाता है, दो मार्गों को दर्शाता है जिन पर लोगों के जीवन आगे बढ़ सकते हैं — एक मार्ग वह है जो मूर्खों के प्रभाव में होता है, और दूसरा वह है जहाँ व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान लगाता है और इस बुद्धि को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनता है। मूर्खता का मार्ग उस जीवन की ओर ले जाता है जो हवा में उड़ती धूल के समान है। बुद्धिमानी का मार्ग उस वृक्ष के समान है, जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और जो कई वर्षों तक फल देता है।
यीशु उपदेश के आरम्भिक भाग में यही बात कह रहा है। दाऊद के अन्तिम और विश्वासयोग्य पुत्र, परमेश्वर के राज्य के राजा और स्वयं बुद्धि से परिपूर्ण देहधारी के रूप में, यीशु सभी लोगों को संसार में जीने का वह मार्ग दिखाता है, जो सच्चे आनन्द की प्रतिज्ञा करता है, और न केवल इस युग के लिए, वरन् आने वाले अनन्त जीवन के लिए भी प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार यीशु ने अपने उपदेश का आरम्भ किया, जिसमें उसने सच में अच्छे जीवन के विषय में नौ धन्य वचन कहे।
कम से कम 1,500 वर्षों से, इन आरम्भिक मैकरिज्म को “धन्य वचन” कहा जाता है। यह वर्णन लैटिन शब्द बीट्स से आया है जिसका अर्थ मकारियोस के समान है — अर्थात् “आनन्द” या “फलना-फूलना”। मसीहियों ने हमेशा मत्ती 5:3–12 को उस सच्चे फलते-फूलते जीवन के निमंत्रण के रूप में समझा है, जो केवल यीशु के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वही यीशु, जिसने यूहन्ना की पुस्तक में यह कहा कि वह इसलिए आया “कि वे जीवन पाएँ, और बहुतायत से पाएँ” (यूहन्ना 10:10)।
परन्तु आजकल इस बात को लेकर बहुत अधिक भ्रम है कि धन्य वचन क्या हैं। लगभग प्रत्येक आधुनिक अंग्रेज़ी बाइबल में यीशु के मकारियोस कथनों का अनुवाद अंग्रेज़ी शब्द “धन्य” के साथ किया गया है। “धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं… धन्य हैं वे जो शोक करते हैं,” आदि। यह एक बिल्कुल अलग विचार है। यदि हम यीशु के धन्य वचनों को आशीष वचनों के रूप में पढ़ते हैं, तो हमें यह पूछना होगा कि इसका अर्थ क्या है। क्या यीशु यह कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा जो 5:3-12 में वर्णन किए गए तरीकों से जीवन जीते हैं? क्या ये राज्य में प्रवेश करने के लिए नई माँग है? या ये केवल उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें राज्य के आने पर परमेश्वर आशीष देगा (जो अभी भी एक माँग के ही समान है)? ये प्रश्न आनन्द और फलना-फूलना के स्वभाव को गलत समझते हैं। धन्य वचनों के द्वारा यीशु हमें अपनी उस सच्ची समझ को अपनाने के लिए कहता है, जिस के द्वारा हम सच्चा जीवन पा सकें। यह न तो प्रवेश करने की माँग है और न ही भविष्य के विषय में केवल एक कथन है। यह एक नया दृष्टिकोण है कि कैसे परमेश्वर का अनुसरण करके सच्चा जीवन पाया जा सकता है।
चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि यीशु हमें सच्चे फलते-फूलते जीवन का चित्र दिखाता है, वरन् यह है कि वह परमेश्वर के राज्य में इस जीवन का वर्णन किस प्रकार से करता है। यीशु का आनन्द एवं फलना-फूलना का अर्थ बिल्कुल भी वैसा नहीं हैं जैसे हममें से कोई अपेक्षा करेगा या स्वाभाविक रूप से चाहेगा। जब हम यीशु के नौ वचनों को पढ़ते हैं कि सच्चा जीवन कहाँ पाया जा सकता है, तो एक को छोड़कर शेष वचन अप्रत्याशित रूप से नकारात्मक प्रतीत होते हैं!
- फलते-फूलते [“धन्य”] हैं वे जो मन के दीन हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो शोक करते हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो नम्र हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो दयालु हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो मन के शुद्ध हैं… [एकमात्र संभावित सकारात्मक वचन]
- फलते-फूलते हैं वे जो मेल-मिलाप करवाने वाले हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं…
- फलते-फूलते हैं वे जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्दा करें और सताएँ और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें…
इस चित्रण पर ध्यान दें – निर्धनता, शोक, विनम्रता, भूख-प्यास, और सताव। मेल-मिलाप और दया की धारणाएँ अधिक सकारात्मक प्रतीत हो सकती हैं, परन्तु ये भी दूसरों के साथ सम्बन्धों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने अधिकारों को त्यागने के नकारात्मक चित्रण है।
यहाँ क्या हो रहा है? यीशु के द्वारा कहे गए फलने-फूलने वाले वचन को समझने के लिए, दूसरे भाग में उसके द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:
- … क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
- … क्योंकि वे शान्ति पाएँगे।
- … क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
- … क्योंकि वे तृप्त किए जाएँगे।
- … क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
- … क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
- … क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएँगे।
- … क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
हमें आमंत्रित करते हुए यीशु हमारे अच्छे जीवन की धारणाओं को फिर से ढाल रहा है, ताकि हम अपने जीवन का सम्बन्ध परमेश्वर के साथ बना कर रखें, क्योंकि वही हमें वह सब कुछ देगा, जिसकी हम इच्छा करते है और जिसकी हमें आवश्यकता भी है। वह यह कह सकता है कि ये नकारात्मक अवस्थाएँ — नम्रता, शोक, सामर्थ्य को खोना, दूसरों को क्षमा करने के लिए अधिकार त्यागना, गलत रीति से बुरी बातें सहना और सताव को अपनाना — ये सब आनन्द है, क्योंकि इन परिस्थितियों में हमारे मन परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और वह हमें वहीं मिलता है। यीशु कह रहा है कि सच में अच्छे जीवन की कुंजी इस बात में सम्मिलित है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर और उसके राज्य की ओर फिर से मोड़ दें (देखें मत्ती 6:33) — इसमें यह भी सम्मिलित है कि सच्चे आनन्द के बीच में दुख, हानि और शोक का भी सामना करना पड़ेगा।
यही मत्ती 5:13–16 में प्रसिद्ध “नमक और ज्योति” वाली आयत का अर्थ है। यीशु अपने शिष्यों को संसार में अपने स्वयं के मार्ग पर चलने के लिए बुला रहा है, ताकि वे उस नई वाचा के सन्देश वाहक बनें जिसे वह संसार में ला रहा है। क्योंकि इससे विरोध और हानि होगी (विशेषकर मत्ती 10 देखें), उसके शिष्य यीशु के मार्ग से पीछे हटने, नमक का स्वाद खोने और अपने उजियाले को ढकने के लिए परीक्षा में पड़ सकते हैं। परन्तु यह शिष्यत्व का मार्ग नहीं है। इसके विपरीत यीशु कहता है कि, “उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में हैं, बड़ाई करें” (5:16)।
अतः यहाँ मार्गदर्शन का सन्देश क्या है?
हम सभी एक सार्थक और आनन्दमय जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। यीशु और बाइबल इसके विरोध में नहीं हैं। वास्तव में, यीशु नए नियम में अपना पहला उपदेश इसी सन्देश के साथ आरम्भ करता है। हमारी समस्या आनन्द की इच्छा होना नहीं है, वरन् हमारी मूर्खता और अन्धापन है, जो इस आनन्द को परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर ढूँढने का प्रयास करता है। जैसा कि सी.एस. लुईस ने से कहा जो कि उनका प्रसिद्ध कथन था कि,
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रभु को हमारी इच्छाएँ बहुत प्रबल नहीं, वरन् बहुत निर्बल सी दिखाए देती हैं। हम आधे-अधूरे मन वाले प्राणी हैं, जो असीमित आनन्द मिलने के प्रस्ताव पर भी शराब, यौन सम्बन्ध और महत्वाकाँक्षा में मग्न रहते हैं, और उस अनन्त आनन्द की खोज करने के विपरीत हम सीमित सुखों से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं क्योंकि यह मानवीय प्रवृत्ति है। हम बहुत शीघ्र ही सन्तुष्ट हो जाते हैं।(“द वेट ऑफ ग्लोरी”)
यहाँ उपदेश के आरम्भ में, यीशु हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके मार्गदर्शन का जूआ उठाएँ और परमेश्वर तथा उसके आने वाले राज्य के आस-पास अच्छे जीवन के लिए अपनी धारणाओं को पुनः ढालें, तथा दया, विनम्रता, सताव सहने तथा यीशु के उस नमूने का पालन करें जिसका नमूना स्वयं यीशु ने दिया है।
चर्चा एवं मनन
- यीशु के धन्य वचन की यह व्याख्या, आपकी पिछली समझ से किस प्रकार समान है या भिन्न है?
- हमें यीशु के मार्गदर्शन का जूआ क्यों उठाना चाहिए — क्या हमें पहाड़ी उपदेश की बुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए?
3
दूसरे लोगों के साथ हमारे सम्बन्धों को लेकर परमेश्वर किस बात की चिन्ता करता है? (5:17–5:48)
मसीहियों के लिए सबसे अधिक उलझन भरे और जटिल प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है कि पुराने नियम और उसकी शिक्षाओं को नए नियम के साथ किस प्रकार से समझा जाए और उनका आपस में क्या सम्बन्ध है। क्या पुराने नियम की आज्ञाएँ आज भी मसीहियों पर लागू होती हैं? क्या परमेश्वर नए नियम में भी अपने लोगों से वही अपेक्षा करता है, जो उसने पुराने नियम में की थी?
विभिन्न ईश्वर विज्ञानियों और सम्प्रदायों ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं, और दो हज़ार वर्षों के मनन एवं चिन्तन के पश्चात् भी इसका का कोई अन्तिम समाधान नहीं हुआ है। ये केवल शैक्षणिक प्रश्न ही नहीं हैं। ये इस बात को भी प्रभावित करते हैं कि हम परमेश्वर के विषय में कैसे सोचते हैं, यदि कोई हों, तो पुराने नियम के कौन से भाग नई वाचा में प्रतिदिन परमेश्वर के लोगों पर लागू होते हैं।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न यीशु के उपदेश के मुख्य भाग (5:17–7:12) के केन्द्र में हैं। हम इस दुविधा का पूरा समाधान केवल इन आयतों से नहीं कर सकते हैं; इसके अर्थ को समझने के लिए हमें सम्पूर्ण नए नियम की आवश्यकता है। परन्तु उपदेश का यह भाग इन प्रश्नों के प्रति मसीहियत के उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
यीशु 5:17 में सीधे तोराह (मूसा की व्यवस्था) और उसका मसीहियत से सम्बन्ध होने के विषय को सम्बोधित करता है, “यह न समझो, कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने आया हूँ।” इस गहन कथन में, यीशु एक साथ इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने इस्राएल के इतिहास में क्या भलाई की और क्या आज्ञा दी, तथा यह भी संकेत करता है कि उसके द्वारा कुछ नया और भिन्न होने वाला है। यीशु पुराने नियम/यहूदी धर्म और मसीहियत के बीच निरन्तरता और अनिरन्तरता दोनों की पुष्टि करता है। वह उन्हें समाप्त नहीं कर रहा है, वरन् उन्हें पूरा कर रह है।
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के विषय में यीशु 5:17–7:12 में जो बहुत-सी बातें कहता है, वे इस निरन्तरता और अनिरन्तरता को स्पष्ट करती हैं और उसका स्वरूप भी समझाती हैं। यह अनिरन्तरता इस बात में पाया जाता है कि यीशु स्वयं परमेश्वर की इच्छा का अन्तिम निर्णायक और व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है। वह अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से यह घोषणा करता है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की व्याख्या कैसे करनी चाहिए (“तुमने यह सुना, परन्तु मैं तुम से कहता हूँ…”)। उपदेश के अन्त में, यीशु फिर से यह दोहराता है कि अब उसके वचन ही अन्तिम वचन हैं: “इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया” (7:24)।
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को आगे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु लगातार ईश्वरीय अधिकार का दावा करता है, जैसे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य (9:6), स्वयं प्रकृति पर नियंत्रण करना (14:13–33), और यह घोषणा करना कि उसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता है (11:25–27)। यह “स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार” जो उसके पुनरुत्थान के बाद पूरी रीति से उसके पास है (28:18-20) उसे उसकी कलीसिया को, अर्थात् संसार भर में उसके शिष्यों के समूह को निरन्तर सौंपा जाता है (18:18-20; 10:40; 21:21)। यह सब अनिरन्तरता है। एक नया युग है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक नई वाचा है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो विश्वास से उसका अनुसरण करता है (26:28), चाहे वह यहूदी हो या गैर-यहूदी, मूसा की पुरानी वाचा से अलग है (रोमियों 3:21-26; गलातियों 3:15-29; इब्रानियों 9:15-28)।
परन्तु परमेश्वर ने अतीत में जो कहा था और यीशु अब जो सिखा रहा है, उनके बीच निरन्तरता बनी हुई है। परमेश्वर नहीं बदला है, उसकी इच्छा और उसकी धार्मिकता नहीं बदली है। मसीही लोग एक नई वाचा का हिस्सा हैं, जिसमें मसीह मध्यस्थ है। परन्तु परमेश्वर अपने लोगों से जो चाहता है उसके लिए उसका हृदय नहीं बदलता है, क्योंकि वह कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देता जो उसके स्वभाव के अनुरूप न हो। मूसा की वाचा के विशेष यहूदी पहलू समाप्त हो गए हैं क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है — अर्थात उस “वंश” (यीशु) को प्रकट करना, जो अब्राहम से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा जिससे सब जातियाँ आशीष पाएँ (गलातियों 3:15–29)। परन्तु एक नई वाचा है, जिसमें हर किसी — चाहे यहूदी हो या अन्यजाति — को सम्मिलित होना आवश्यक है ताकि वे परमेश्वर के लोग कहलाए जाएँ। परन्तु अपनी सृष्टि के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं बदली है। यही बात 5:17–7:12 का सार है।
यहाँ यीशु की सारी शिक्षाओं के ऊपर जो वचन छाया हुआ है और जो उन्हें दिशा देता है, वह 5:20 में पाया जाता है: “यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे।” पहली दृष्टि में यह ऐसा लग सकता है मानो यीशु कह रहा है कि हमें पुराने नियम के पवित्र लोगों से, और विशेषकर अत्यधिक धार्मिक फ़रीसियों से भी अधिक बढ़कर धार्मिकता के कार्य करने होंगे। यह कोई सुखद सम्भावना नहीं है। और न ही यह यीशु का उद्देश्य है, वरन् उसका उद्देश्य यह है कि हमारे पास ऐसी धार्मिकता होनी चाहिए जो केवल बाहरी रूप (व्यवहार) तक सीमित न हो, वरन् आन्तरिक (मन में) भी हो। “वह धार्मिकता जो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है” अर्थात् बाहरी और आन्तरिक दोनों है।
जैसा कि पुराने नियम में कहा गया है; कि परमेश्वर सदैव हमारे मन को देखता और उसकी चिन्ता करता है, न कि केवल हमारे कार्यों की। पवित्र होने का अर्थ ही सम्पूर्ण होना है। मरे हुए मन से भले कार्य करना परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए हमें भी पूर्ण/स्थाई बने रहना चाहिए, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण/स्थाई बना हुआ है (5:48 में यही “सिद्ध” होने का अर्थ है)। यही वह शिक्षा है जो यीशु 5:17–7:12 में सिखा रहा है।
अतः 5:17-48 में मार्गदर्शन का सन्देश क्या है?
सरल शब्दों में कहें तो, यीशु के द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले शिष्य का अर्थ यह है कि हमें अपने मन के भीतर झाँकना चाहिए, न कि केवल अपने बाहरी अच्छे व्यवहार पर ध्यान लगाना चाहिए। यीशु इस पूरे व्यक्ति की “बड़ी धार्मिकता” की धारणा को उन छह तरीकों से लागू करता है जिनसे हम दूसरों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। निम्नलिखित सूची कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह सूची पूरी रीति से निर्देशों का समूह नहीं हैं, परन्तु इसका उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बन्ध रखते समय हमारे मन के महत्व के विषय में हमारी सोच को पुनः प्रशिक्षित करना है।
- पहला उदाहरण क्रोध, कड़वाहट और दूसरों के प्रति घृणा से सम्बन्धित है (5:21–26)। यीशु स्वीकार करता है कि हत्या करना ग़लत है। परन्तु वह हत्या के अन्तिम कृत्य के अन्तर्गत आने वाले मन के विषय पर बल देता है—अर्थात् किसी दूसरे के प्रति क्रोध और बदले की भावना होना। वह अपने शिष्यों को चुनौती देता है कि वे अपने भीतर देखें और मूल समस्या का समाधान करें।
- दूसरा और तीसरा उदाहरण कामुकता के शक्तिशाली मानवीय अनुभव और विवाह में इसके परिणाम से सम्बन्धित है (5:27-32)। यीशु ने इस बात की पुष्टि की कि व्यभिचार गलत है। परन्तु जब शिष्यों का हृदय वासना से भरा हो, तो वे इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकते कि उन्होंने व्यभिचार नहीं किया है (5:27-30)। शिष्य विवाह के पवित्र बन्धन के साथ कठोर मन से व्यवहार नहीं सकते हैं और इस प्रकार मूर्खता पूर्ण तलाक नहीं ले सकते हैं (5:31-32; 19:1-10 में आगे का स्पष्टीकरण देखें)।
- चौथे उदाहरण में, यीशु इस बात को सम्बोधित कर रहा है कि हम अपने शब्दों के पालन करने में सम्पूर्ण व्यक्ति कैसे बन सकते हैं (5:33–37)। यदि कोई बाहरी समर्पणता या प्रतिज्ञा करता है, तो उसे आन्तरिक इच्छा के साथ मेल खाना चाहिए कि वह जो कह रहा है, उसे पूरा भी करे।
- पाँचवें और छठे उदाहरण में, यीशु सबसे कठिन सम्बन्धों में सिद्धता की आवश्यकता पर बल देता है — अर्थात् जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और साथ ही जो हमारे शत्रु भी हैं (5:38-48)। दोनों ही सन्दर्भ में, यीशु अपने शिष्यों को प्रतिशोध लेने के हृदय से प्रेम के हृदय की ओर बढ़ने के लिए कहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता अपने बच्चों और शत्रुओं के प्रति दयालु है, ठीक उसी प्रकार यीशु के शिष्यों को भी अपने शत्रुओं के प्रति दयालु होना चाहिए।
चर्चा एवं मनन:
- परमेश्वर केवल हमारे कार्यों को ही क्यों अपने वचन के अनुरूप नहीं चाहता है?
- मत्ती 5:17–48 ने आपके सम्बन्धों के विषय में आपको किस प्रकार से चुनौती दी है?
4
परमेश्वर हमारे और अपने सम्बन्ध में किस बात की चिन्ता करता है?
(6:1–21)
5:17-20 में, यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह जो सिखा रहा है वह परमेश्वर के द्वारा अतीत में कही गई बातों के विपरीत नहीं है। वह नई वाचा ला रहा है, जो यह पुनः परिभाषित करती है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं और परमेश्वर तक कैसे पहुँचा जा सकता है — अर्थात् केवल उसी के द्वारा पहुँचा जा सकता है। परन्तु परमेश्वर जिस धार्मिकता की माँग करता है, वह नहीं बदली है। इसलिए हमें न केवल अपने बाहरी व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वरन् अपने हृदय में भी परिवर्तन लाना होगा। अब यीशु इसे परमेश्वर को सम्मान देने के लिए की जाने वाले हमारे आत्मिक अभ्यास पर भी लागू करता है।
मत्ती 6:1 में यीशु स्पष्ट रूप से कहता है कि सिद्धता/बड़ी धार्मिकता का सिद्धान्त हमारे आत्मिक अभ्यास पर कैसे लागू होता है। शिष्यों को न केवल अपने अभ्यास पर, परन्तु अपने उद्देश्यों पर भी सावधानी के साथ ध्यान देने वाला होना चाहिए: “सावधान रहो! तुम मनुष्यों को दिखाने के लिये अपने धार्मिकता के काम न करो।” हमारे हृदय के स्तर के उद्देश्यों का महत्व है, न कि केवल वे कामों का जो हम करते हैं।
यीशु हमारी भक्ति पूर्ण जीवन जीने के अच्छे और बुरे तरीक़ों के तीन वास्तविक उदाहरण देता है: हमारा दान देना, हमारी प्रार्थना करना और हमारा उपवास रखना। यह आत्मिक कार्यों की कोई विस्तृत सूची नहीं है, वरन् यह इस बात का नमूना है कि जो वह सिखा रहा है, उसे कैसे कार्यान्वित किया जाए। इनमें से प्रत्येक आत्मिक कार्य अच्छे हैं; यीशु उनकी आलोचना नहीं कर रहा है। परन्तु प्रत्येक कार्य में शिष्यों को अपने आन्तरिक उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए।
मत्ती 6:2–4 में यीशु निर्धनों और असहाय लोगों को दान देने की अच्छी प्रथा के विषय में बताता है। भिक्षा देना दशमाँश और अन्य प्रकार के दान से भिन्न होता है, जो मन्दिर या कलीसिया में सहायता करने के लिए दिया जाता है। यह लोगों की विशेष आवश्यकताओं के लिए त्याग पूर्ण दान होता है। भिक्षा देना उन निर्धन लोगों की देखभाल का एक हिस्सा है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने सम्पूर्ण पुराने नियम में दी है (व्यवस्थाविवरण 15:7–11; भजन संहिता 41:1; गलतियों 2:10; याकूब 2:14–17)। यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु यीशु यह बताता है कि इस भले कार्य को खुलकर और दिखावे के साथ करना सम्भव है, ताकि दूसरे लोगों से आदर और प्रशंसा मिल सके। परन्तु सच्चे शिष्य इस प्रकार के दिखावे का विरोध करेंगे और निर्धनों की सहायता ऐसे तरीक़ों से करेंगे जिसमें उनकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा न हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि सारे दान अनिवार्य रूप से छिपाकर ही दिए जाएँ ताकि कोई न जान सके कि पैसा किसने दिया। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यदि हम किसी का सामान इधर-उधर रखने में सहायता करते हैं, तो हमें चेहरा ढककर या गाड़ी की नम्बर प्लेट हटाकर या अपनी आवाज़ बदलकर करना होगा ताकि कोई न जान सके कि सहायता करने वाले हम हैं। परन्तु इसका अर्थ यह है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए स्वयं को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए।
6:5–6 में यीशु हमारे प्रार्थना जीवन के विषय में बात करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्धनों की सहायता करने में दान देने समय यह बहुत अधिक सम्भव है कि हम प्रार्थना भी उसी प्रकार से करें कि दूसरों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हो सके। एक बहुत ही कुशल प्रार्थना करने वाला बनना सम्भव है, जिसकी बोलने की प्रभावशाली कला और सार्वजनिक रूप से बार-बार प्रार्थना करना स्वयं के प्रचार का स्रोत बन जाता है। यीशु के शिष्यों को इस प्रलोभन का विरोध करना चाहिए, और पिता से विश्वासयोग्यता के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दिखाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दान देने के समान इसका यह अर्थ नहीं है कि हम कभी भी सार्वजनिक या सामूहिक रूप से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पुराना और नया नियम तथा कलीसिया का इतिहास दूसरों के साथ प्रार्थना करने के अच्छे नमूनों से भरा हुआ है। परन्तु इसका अर्थ यह है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि कहीं प्रार्थना करने के पीछे सम्मान पाने का उद्देश्य तो नहीं है।
जब यीशु इस विषय पर बोल रहा था, तो वह और आगे बढ़कर इस बात पर बल देता है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए वह हमें जो प्रार्थना सिखाता है उसे “प्रभु की प्रार्थना” कहा जाता है (6:9–13)। यीशु के शिष्यों को परमेश्वर के पास वैसे नहीं जाना चाहिए जैसे अन्यजाति के लोग जाते हैं जो बहुत सारे शब्दों को बड़बड़ाते हैं, मानो किसी दूर बैठे परमेश्वर को मनाने का प्रयास कर रहे हों कि वह उनकी सुन ले, जैसे कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र हो (6:7)। वरन् मसीही लोग परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं, जैसे यीशु जानता है, इसलिए हम अलग रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना में, यीशु उस प्रकार की प्रार्थना के लिए अगुवाई कर रहा है जो दिखावे के लिए नहीं, परन्तु सच्ची और परमेश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करके की जाती है।
मत्ती 6:18–19 में यीशु सम्पूर्ण व्यक्ति की ईश्वरीय भक्ति का तीसरा उदाहरण देता है, और इस बार वह उपवास के विषय में बताता है। उपवास — भोजन से एक निश्चित समय के लिए परहेज करना है ताकि हम उस पर निर्भर होने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकें — यहूदियों और मसीहियों द्वारा हज़ारों वर्षों से ऐसा किया जाता रहा है। यीशु अपने शिष्यों से इस अभ्यास को करने की अपेक्षा करता है और उसकी सराहना भी करता है। परन्तु जैसे दान देने और प्रार्थना करने में होता है, वैसे ही उपवास के इस अच्छे अभ्यास को भी दूसरों से सम्मान पाने के लिए करना बहुत सरल हो जाता है। ऐसा उपवास रखना सम्भव है जो किसी की भक्ति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर दे। इसके विपरीत यीशु अपने शिष्यों को उपवास के एक अलग तरीके के लिए कहता है, जो बाहरी दिखावे पर नहीं, वरन् पिता के रूप में परमेश्वर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध पर ध्यान केंद्रित करता है।
यीशु ने भक्ति के कार्यों में हमारे हृदयों पर ध्यान देने की इस तीन स्तरीय चर्चा को अन्तिम उपदेश के साथ समाप्त किया: “अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो; जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं।परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा, और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं (मत्ती 6:19-20)। यह उस बात को कहने का एक और तरीका है जो उसने 6:1 में कही थी, जब उसने चेतावनी दी थी कि, यदि तुम गलत उद्देश्य के साथ ईश्वर भक्ति करते हो, “तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे।” प्रत्येक उदाहरण में यीशु एक ही भाषा का उपयोग करता है — मन की भावनाएँ ही यह अन्तर उत्पन्न करती हैं कि कोई स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाएगा (6:4, 6, 18) या फिर लोगों की प्रशंसा का अस्थायी और क्षणभंगुर “प्रतिफल,” जो वास्तव में कोई प्रतिफल है ही नहीं (6:2, 5, 16)।
अतः 6:1–21 में मार्गदर्शन का क्या सन्देश है?
एक बार फिर: यीशु का शिष्य होने का अर्थ यह है कि हमें केवल अपने अच्छे व्यवहार पर ही नहीं, वरन् अपने मन के भीतर भी देखना चाहिए। ईश्वर भक्ति के कार्य — जैसे दान देना, प्रार्थना करना और उपवास रखना — अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे जीवन को आकार देते हैं। परन्तु यदि हम अपने मन और भावनाओं की जाँच नहीं करेंगे तो ऐसी बाहरी धार्मिकता अपर्याप्त है। फरीसी हमें यह नमूना दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति एक अच्छा धार्मिक मनुष्य तो हो सकता है, परन्तु वास्तव में परमेश्वर पिता के साथ उसका सम्बन्ध नहीं होता है।
एक बार जब हम यीशु से यह सन्देश सुनना आरम्भ करते हैं, तो निराशा और मनोबल का गिरना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति जानता है कि उद्देश्य कभी भी पूरी रीति से स्पष्ट और शुद्ध नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब हम पूर्ण सच्चाई की खोज करते हैं, तो हमारा दूसरों को दान देना, हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारी शिक्षा, हमारा सुसमाचार प्रचार, आदि कभी भी एक-दूसरे के साथ जुड़े होने से स्वतंत्र नहीं होते हैं। यीशु का उद्देश्य हमें स्वयं की जाँच करने के लिए निकम्मा बनाना नहीं है जो हमें तब तक भले कार्य करने से रोकता है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमारा मन पूरी रीति से शुद्ध है। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि हम नई सृष्टि में पूरी रीति से छुटकारा नहीं पा लेते हैं। इसके विपरीत, यीशु अपने शिष्यों को उनके मनों के प्रति सचेत रहने के लिए कहता है। जब हम अपने जीवन में उसके शिष्यत्व का जूआ उठाते हैं, तो यह हमारे उद्देश्यों, संवेदनाओं और स्नेह को आकार देगा। हमारे जीवन में उन्नति करने तथा दुःखी होने का समय आएगा। हम अपने हृदय के एक क्षेत्र में उन्नति करेंगे और अन्य क्षेत्रों में ठोकर खाएँगे। परन्तु समय के साथ हम उनसे सीखते हुए सिद्ध होने में उन्नति भी देखेंगे।
मनन के लिए प्रश्न
- अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर को अपना “स्वर्गीय पिता” मानकर प्रार्थना करना कैसा होगा?
- आप किस प्रकार से परमेश्वर का आदर करने के विपरीत लोगों से प्रशंसा और आदर पाने के लिए आत्मिक कार्य करने के लिए परीक्षा में पड़ते हैं?
- क्या आप यीशु की आज्ञा मानने में संघर्ष करते हैं जबकि आपको पता होता है कि आपके उद्देश्य पूरी रीति से शुद्ध नहीं हैं? फिर भी आपको विश्वासयोग्यता के साथ अगला कदम क्यों उठाना चाहिए?
5
संसार की वस्तुओं और लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध के विषय में परमेश्वर किस बात की चिन्ता करता है? (6:19–7:12)
पुराने यूनानी लेखन कार्यों में, लेखक अधिकाँश शब्दों का चतुराई से उपयोग करते थे, एक ही शब्द का उपयोग करके दो अलग-अलग विचार प्रकट कर देते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम आज भी कविता और गीतों में करते हैं। मत्ती 6:19-21 में, यीशु ठीक ऐसा ही करता है। पृथ्वी पर धन इकट्ठा के स्थान पर, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के उपदेश में आत्मिक प्रतिफलों के विषय में यीशु के द्वारा कही गई बात का यही निष्कर्ष है 6:1-18। साथ ही, पृथ्वी पर नहीं, परन्तु स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन भी सम्मिलित है 6:22–7:12।
उपदेश के इस मुख्य तीसरे भाग (6:19–7:12) में, यीशु उसी सन्देश को आगे बढ़ाते हुए कहता है— धर्मी होना केवल बाहरी भक्तिमय व्यवहार करना नहीं है; परन्तु ईश्वरीय भक्ति एक परिवर्तित हृदय से होनी चाहिए। केवल ऊपरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं है (5:20)। इसके विपरीत, शिष्य होने का अर्थ सिद्धता की खोज करना है— अर्थात् अन्दर और बाहर दोनों ओर से पिता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए (5:48)।
6:19-7:12 में यीशु सिद्धता को शिष्यों के साथ संसार की वस्तुओं, संसार के लोगों, धन और सम्बन्धों पर लागू करता है। जिस धन को हम इकट्ठा करके रखते हैं, उसी से हम प्रेम करने लगते हैं और भीतर से वही हमारी पहचान बन जाती है। यही यीशु का भी अर्थ है जब वह कहता है कि, “”क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा।” (6:21)। यीशु सबसे पहले यह बताता है कि यह मन रूपी धन का सिद्धान्त शिष्य के धन के सम्बन्ध में कैसे कार्य करता है। एक ऐसी उपमा का उपयोग करते हुए यीशु कहता है कि आधुनिक पाठक उससे कम ही परिचित हैं, कि धन में हमारे मन को लोभ और ईर्ष्या की ओर मोड़ने की योग्यता होती है। बुरी या लालची आँख पूरे शरीर को अन्धकारमय कर देती है (6:22–24)। इसके पश्चात् वह धन और परमेश्वर दोनों की सेवा करने के प्रयास को दो अलग-अलग स्वामियों की सेवा करने के समान असम्भव कार्य बताता है। क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि एक के प्रति निष्ठावान बना रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा; परमेश्वर और धन दोनों से सच में प्रेम रखना सम्भव नहीं है (6:24)।
इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, यीशु धन और उससे मिलने वाली सभी वस्तुओं के विषय में, चिन्ता के विषय को सम्बोधित करता है (6:25-34)। निस्संदेह मनुष्य का जीवन सदैव चिन्ताओं और व्याकुलता से भरा रहता है; अपने भविष्य, अपने बच्चों और नाती-पोतों, मित्रों, कलीसिया, देश और विश्व के विषय में चिन्ता होना बहुत स्वाभाविक है। यीशु न तो स्वाभाविक चिन्ताओं की निन्दा कर रहा है, और न ही बिना भावनाओं के जीवन जीने की सलाह दे रहा है। परन्तु वह यह बता रहा है कि जब हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम वह सुरक्षा और आनन्द नहीं होता है जिसकी हम आशा करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि हम पिता पर भरोसा करते हैं, और स्वयं ही अपनी देखभाल करने का प्रयास करते हैं, तो परिणाम वह सुरक्षा और शान्ति नहीं होती जिसके विषय में हम सोचते हैं कि इससे मिलेगी। इसके ठीक विपरीत, इस प्रकार की दोहरी मानसिकता चिन्ता उत्पन्न करती है। धन और उससे मिलने वाली सभी वस्तुओं के विषय में चिन्ता करना वर्तमान और काल्पनिक भविष्य के बीच विभाजित जीवन शैली जीने का होने वाला निश्चित परिणाम है। आत्मा का यह विभाजन सिद्ध होने के विपरीत है (5:48) और इसलिए इससे समृद्धि नहीं आएगी, वरन् और अधिक अनिश्चितता आएगी।
परमेश्वर और धन से प्रेम करने के इस चिन्ताजनक प्रयास से बचने के दो तरीके हैं। यीशु के शिष्यों को अपने स्वर्गीय पिता की देखभाल और प्रावधान को सचेत रूप से स्मरण रखना चाहिए, और अपने हृदय तथा जीवन को समर्पित करते हुए आने वाले राज्य की ओर पुनः उन्मुख चाहिए।
स्वर्गीय पिता की देखभाल को स्मरण करने के लिए हमें सृष्टि से आगे कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। पक्षियों के पास खेत में बोने की योग्यता नहीं होती है, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन उपलब्ध करता है (6:26)। फूलों के पास कपड़े सिलने की योग्यता नहीं होती, फिर भी परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है (6:28–29)। परमेश्वर की सन्तान क्षणभंगुर पक्षियों और मुरझा जाने वाले फूलों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए, हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें अपने चिन्तित हृदय को शान्ति दिलाने के लिए उसकी पिता समान देखभाल को सचेत होकर स्मरण करना चाहिए।
अंततः हमें अपने परिश्रम, समय की समर्पणता और धन का उपयोग भी सचेत होकर राज्य की प्राथमिकताओं की ओर पुनः केंद्रित करना चाहिए। यीशु अपने शिष्यों को आमंत्रित करता है कि वे “पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें,” और यह प्रतिज्ञा करता है कि जब हम ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रतिदिन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा (6:33)।
मत्ती 7:1–6 में यीशु हमें आगे सिखाता है कि राज्य के शिष्य वे हैं जो दूसरों का मूल्याँकन और न्याय करते समय दीनता से अपने मन की जाँच करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना और दूसरों की आलोचना करके अपनी पहचान को दृढ़ करने का प्रयास करना न तो जीवन का मार्ग है और न ही वह ऐसी धार्मिकता है जो शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है (5:20)। हमें सही दिशा दिखाने के लिए यीशु गम्भीर चेतावनी देता है कि देर-सबेर जिस प्रकार से हम दूसरों का मूल्याँकन करते हैं, उसी प्रकार न्याय के साथ हमारा भी मूल्याँकन किया जाएगा (7:1)। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, यीशु एक ऐसे व्यक्ति की हास्यपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है जो किसी दूसरे की आँख से तिनका निकालने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसकी स्वयं की आँख में लट्ठा पड़ा हुआ है (7:1-5)। यह हमें यीशु के उस सेवक के दृष्टान्त का स्मरण कराता है जिसे बहुत अधिक क्षमा किया गया था, परन्तु उसने अपने संगी दास को क्षमा करने से मना कर दिया (मत्ती 18:21-35)। यीशु के शिष्य वे हैं जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए बुद्धिमानी से चलते हैं (7:6) और जिनका जीवन दया, करुणा और क्षमा से पहचाना जाता है (5:7, 9, 21–26, 43–48)।
उपदेश के मुख्य भाग को समाप्त करते हुए यीशु अपने शिष्यों से स्वर्गीय पिता की अनुग्रहपूर्ण देखभाल के विषय में बड़ी शान्ति और प्रोत्साहन देने वाले वचन बोलता है (7:7–11)। परमेश्वर पिता प्राचीन संसार के अन्य देवताओं के समान — अर्थात् चंचल, अविश्वसनीय और हमेशा से अज्ञात नहीं हैं। वरन् वह ऐसा पिता है जो हर्षपूर्वक, उदारता तथा पूरे मन से अपनी सन्तान को अच्छे वरदान देता है। हमें तो केवल माँगना है।
संसार की वस्तुओं और लोगों के साथ सम्पूर्ण हृदय से जीवन जीने के विषय में यीशु की सभी शिक्षाओं (मत्ती 6:19–7:12) का सार यीशु के इस स्मरणीय वचन में समेटा जा सकता है, “इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो; क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है” (7:12)। यीशु व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने नहीं, परन्तु उन्हें पूरा करने आया है (5:17)। वह एक नई वाचा स्थापित कर रहा है और परमेश्वर के लोगों को, जो उसके अनुयायी हैं, पुनः परिभाषित कर रहा है। परन्तु परमेश्वर ने हमेशा हमारे भीतरी व्यक्तित्व, हमारे मन को देखा है और उसकी चिन्ता की है। अतः परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के मार्ग पर चलें, परन्तु यह धार्मिकता केवल बाहरी नहीं, वरन् आन्तरिक भी होनी चाहिए। जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, अर्थात् पिता के रूप में परमेश्वर के साथ सम्बन्ध के माध्यम से इस प्रकार की धार्मिकता की खोज करते हैं, तो हम उस समृद्धि या धन्य जीवन को पाना आरम्भ करते हैं जिसके विषय में यीशु ने 5:3-12 में कहा है।
अतः 6:19–7:12 में मार्गदर्शन का सन्देश क्या है?
हमारे जीवन में धन का विषय हमेशा बहुत अधिक व्यक्तिगत होता है। धन, सम्पत्ति और सांसारिक वस्तुएँ ऐसी वास्तविकताएँ हैं जिनसे हर कोई किसी न किसी स्तर पर संघर्ष करता है — और अधिकाँश लोग बड़े स्तर पर संघर्ष करते हैं। जैसा कि देखा गया है, जो व्यक्ति कहता है कि वह धन से प्रभावित नहीं होता है, वह उस शराबी के समान है जो कहता है कि केवल एक और घूँट और पी लूँ । धन और इसके द्वारा हमें मिलने वाली सभी वस्तुएँ हमारे हृदय के स्तर को छूते हैं — जैसे हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान और हमारे मूल्य के सम्बन्ध में।
यीशु धन के साथ हमारे सम्बन्ध को संबोधित करने से पीछे नहीं हटता है, और यह उचित भी है। सिद्धता में आगे बढ़ते हुए सच्ची मानवीय सुख-समृद्धि के लिए उसका निमंत्रण यह अपेक्षा करता है कि हम अपने भीतर देखें और उन तरीकों पर सावधानी के साथ ध्यान दें जिनके द्वारा हम स्वर्ग पर धन इकट्ठा न करने के बदले पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए लालच में पड़ जाते हैं, और जिन तरीकों से हम अधिकाँश एक साथ दो स्वामियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं — अर्थात् परमेश्वर और धन दोनों की। तब इस प्रकार के विभाजित जीवन का परिणाम शान्ति नहीं वरन् चिन्ता होता है। इसलिए मार्गदर्शन प्राप्त शिष्य धन के इस मूल स्तर पर और उन सभी वस्तुओं के विषय में जो यह हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है, यीशु को अपने जीवन में बोलने के लिए तैयार रहेगा/रहेगी, और सचेत होकर निरन्तर “उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज” करने में अपनी समर्पणता को पुनः उन्मुख करेगा/करेगी (6:33)।
इसी प्रकार दूसरों के साथ हमारे सम्बन्धों में भी यही बात लागू होती है। मन से सच्चाई के लिए यह आवश्यक है कि हम उन सभी तरीकों पर ध्यान दें जिनसे हम दूसरों का मूल्याँकन और आलोचना करते हैं। एक मार्गदर्शन प्राप्त शिष्य वह होता है जो दूसरों के प्रति इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विरोध करने में सावधानी पूर्वक कार्य करता है। साथ ही इसके विपरीत, हम दीनता के साथ परमेश्वर को पिता के रूप में देखते हैं और उससे अपनी आँख के लट्ठे को हटाने के लिए कहते हैं।
पिता की अपनी सन्तानों के लिए यही इच्छा है कि वे स्वतंत्रता, शान्ति और संसार की वस्तुओं और लोगों के साथ अपने सम्बन्धों में उन्नति करते रहें। यह तभी सम्भव होगा जब हम अपने मन को इस आन्तरिक कार्य के लिए खोलेंगे जो हमें सिद्धता में बढ़ाता है।
मनन के लिए प्रश्न
- धन और उससे मिलने वाली प्रत्येक वस्तु की चिन्ता आपके जीवन में कैसे उत्पन्न हुई है? किन क्षेत्रों में आपको पहले परमेश्वर के राज्य की पूरी रीति से खोज करने की आवश्यकता है?
- दूसरों की गलतियाँ देखना आसान क्यों होता है, परन्तु अपनी नहीं? आप अपने जीवन में उत्तरदायित्व कैसे ला सकते हैं ताकि आप अपनी आँखों के विभिन्न “तिनकों” को देख सकें?
6
बुद्धि और समृद्धि से भरे जीवन के लिए यीशु का निमंत्रण (7:13-27)
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहाड़ी उपदेश तीन भागों में विभाजित किया गया है — सच्ची समृद्धि और शान्ति का निमंत्रण (5:3–16), सच्ची धार्मिकता का मुख्य विषय, जिसका अर्थ हमारे कार्यों और मन में स्थिरता बनाए रखना है (5:17–7:12), और अन्त में, सच्चा जीवन पाने के लिए निमंत्रणों की एक सूची (7:13–27)। ये सभी भाग अलग-अलग नहीं हैं। इन्हें बुद्धि की शरण में समेटा जा सकता है। बुद्धि, बाइबल की एक बड़ी श्रेणी है जो परमेश्वर की अपने लोगों के लिए इच्छा और उन तरीकों का वर्णन करती है जिनके द्वारा हम परमेश्वर के साथ सकारात्मक सम्बन्ध, शान्ति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। बुद्धि का आरम्भ में परमेश्वर के साथ रहने के रूप में वर्णन किया गया है, जो सभी लोगों को अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों पर पुनः उन्मुख करने के द्वारा जीवन पाने के लिए आमंत्रित करती है (नीतिवचन 8:1-36)। और अंततः, बुद्धि एक व्यक्ति बन जाती है — अर्थात् यीशु मसीह, जो परमेश्वर का देहधारी पुत्र है (1 कुरिन्थियों 1:24; मत्ती 11:25-30 भी देखें)।
सम्पूर्ण पहाड़ी उपदेश को हमें बुद्धि के निमंत्रण के रूप में समझना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे नीतिवचन की पुस्तक, भजन संहिता 1, याकूब की पत्री और बाइबल के कई अन्य भाग भी हैं। यदि अब तक इस उपदेश को सुनने वालों के लिए यह स्पष्ट नहीं हुआ है, तो यीशु के निष्कर्ष में यह पूरी रीति से स्पष्ट हो जाएगा।
सामान्यतः बुद्धि को उसके विपरीत, अर्थात् मूर्खता के साथ तुलना करके दर्शाया जाता है। और हमारे जीवन को एक ऐसे मार्ग के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें लगातार दो मोड़ आते रहते हैं। हम मूर्खता के उस मार्ग को चुन सकते हैं जो हानि, शोक और विनाश की ओर ले जाता है। या फिर हम बुद्धि के उस मार्ग को चुन सकते हैं जो जीवन, समृद्धि और शान्ति की ओर ले जाता है (फिर से भजन संहिता 1 देखें)।
यह “दो प्रकार” की शिक्षा और उपदेश ही है जो हमें यीशु के उपदेश के तीन भाग वाले निष्कर्ष में मिलते हैं:
यीशु का निष्कर्ष: भाग एक
पहले उदाहरण में, वह दो फाटकों और दो मार्गों का वर्णन करता है, जिनमें से एक संकरा और कठिन है तथा दूसरा चौड़ा और सरल है (7:13–14)। किसी भी व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव आसान और सरल मार्ग की ओर होता है, परन्तु यीशु ने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि यह मार्ग जो दिखने में उत्तम प्रतीत होता है वह मार्ग वास्तव में विनाश की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, पथरीला, ऊबड़-खाबड़ और संकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। यह संकरा और कठिन मार्ग क्या है? यह जीवन जीने का वह तरीका है जिसकी यीशु ने अपने पूरे सन्देश में सराहना की है — अर्थात् केवल बाहरी दिखावा करने के लिए धर्मी होना नहीं, वरन् आन्तरिक रूप से सिद्धता में बढ़ने वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करना है।
यीशु का निष्कर्ष: भाग दो
यीशु के दूसरे उदाहरण में “दो-मार्गों” का बहुत विस्तृत वर्णन है और इसमें एक ऐसा सूक्ष्म तत्व जुड़ा हुआ है जो विचार करने योग्य है (7:15–22)। मुख्य विचार यह है कि बुद्धिमान शिष्य इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में क्या मूल्य रखता है। हमारी मानवीय प्रवृत्ति उन लोगों को अधिक महत्व और सम्मान देने की होती है जिनके वरदान और सामर्थ्य दोनों ही दिखावटी होती हैं और बाहरी रूप से प्रभावशाली अभिव्यक्त करने वाली हैं — जिनका यहाँ पर भविष्यवाणी करने, दुष्टात्माओं को निकालने और कई चमत्कार करने के रूप में वर्णन किया गया है (7:22)। प्रेरित पौलुस भी इसी विषय को सम्बोधित करता है, जब वह अन्य बाहरी रूप से प्रभावशाली वरदानों — जैसे कि लोगों के भीतर प्रेम न होते हुए भी अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना, चंगाई देना, ज्ञान की बातें कहना के दुरुपयोग की सम्भावना के विषय में बात करता है, (1 कुरिन्थियों 12–14)। आश्चर्य की बात यह है कि, यीशु कहता है कि ऐसे बहुत से क्षेत्रों में, जो लोग बाहरी रूप से वरदान पाए हुए प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते हैं (7:23)। वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं (7:15)। यीशु कह रहा है कि सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता के बीच का अन्तर बाहरी दिखावटी सामर्थ्य प्रदर्शन में नहीं है (हमें स्मरण कर सकते हैं कि फिरौन के दरबार के जादूगर भी मूसा की कुछ ईश्वरीय सामर्थ्य की नकल करने में सक्षम थे, निर्गमन 7:8-13)। परन्तु सच्चा भविष्यद्वक्ता वह होता है जिसका आन्तरिक जीवन उसके बाहरी जीवन से मेल खाता है, और जिसका व्यवहार अच्छे हृदय से उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति मसीहियत के नाम पर चमत्कार तो कर सकता है, परन्तु भीतर से वह भेड़ नहीं, वरन् भेड़िया होता है, जैसा कि वह दिखाई देता है (7:15)।
मत्ती 7:16–20 में यीशु एक मुख्य विचार दोहराता है: कि किसी भी वृक्ष को उसके फल से पहचाना जाता है। अंजीर का वृक्ष अंजीर ही उत्पन्न करता है, सेब नहीं करता। एक स्वस्थ वृक्ष स्वस्थ एवं पूरा फल देता है, न कि रोगग्रस्त या निकम्मा फल। पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस अनुच्छेद में यीशु द्वारा कही गई बात के विपरीत है! उसने अभी-अभी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो भेड़ जैसा दिखाई देता है और अच्छे काम करता है, परन्तु वास्तव में वह भेड़िया है। तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई वृक्ष अच्छा है या बुरा, यदि भेड़िए भी भेड़ के समान फल उत्पन्न कर सकते हैं? यहीं पर वह महत्वपूर्ण सूक्ष्मता सामने आती है। वृक्ष का यह चित्र हमें स्मरण दिलाता है कि कई बार यह पहचानने में समय लगता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का वृक्ष है और क्या वह वृक्ष वास्तव में स्वस्थ है भी कि नहीं। जब केला और कदली के पौधे जंगल में बढ़ रहे होते हैं, उस समय आप उनमें भेद नहीं कर सकते जब तक कि उनके अलग-अलग प्रकार के फल कली से बाहर न आने लगें। सर्दियों में जीवित और मरे हुए दोनों वृक्ष अधिकाँश एक समान ही दिखाई देते हैं। केवल वसन्त ऋतु में, जब वृक्ष फूल देने लगते हैं, तब ही उनके बीच का अन्तर पहचाना जा सकता है। ऐसा ही संसार में लोगों के साथ भी होता है। देर-सवेर ही सही पर किसी भी व्यक्ति का सच्चा फल और उसका वास्तविक आत्मिक स्वस्थ जीवन प्रकट हो ही जाता है। यह बाहरी धार्मिकता के उदाहरणों से नहीं आएगा—जैसे कि बड़ी ईश्वर भक्ति के कार्य, व्यवस्था का पालन, या चमत्कार करने वाली सामर्थ्य से भी नहीं आएगा, वरन् सच्चे शिष्यों को मन की स्तिथि को देखकर पहचाना जा सकता है। यीशु जिन विषयों की प्रशंसा करता है, वे सबसे पहले मन से जुड़े हुए होते हैं — जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, विश्वासयोग्यता, न कि कामुकता, लोभ, ईर्ष्या, घृणा और घमण्ड से भरा होना। देर-सवेर ही सही पर कभी न कभी ये चरित्र के लक्षण गुण या इनका अभाव प्रकट हो जाएगा और यह दिखा देंगे कि वास्तव में कोई व्यक्ति किस प्रकार का वृक्ष है।
यीशु का निष्कर्ष: भाग तीन
तीसरा और अन्तिम “दो-मार्ग” बुद्धि के लिए निमंत्रण है, जो कि मत्ती 7:24–27 में पाया जाता है। यीशु ने अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश के समापन में जिस छवि का प्रयोग किया है, वह दो अलग-अलग प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिनसे लोग उसके सन्देश पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इनका स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में वर्णन किया जा सकता है: अर्थात् मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। इन दोनों व्यक्तियों का वर्णन एक घर बनाने वाले के रूप में किया गया है, जो स्पष्ट रूप से उनके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है (देखें नीति वचन 8:1, जहाँ बुद्धि को अपना घर बनाने वाला बताया गया है)। बाइबल में पूरे समय बने रहने वाले बुद्धि के विषय को ध्यान में रखते हुए, इन दो प्रकार के लोगों की अन्तिम स्थिति कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मूर्ख व्यक्ति का घर रेत पर बना होता है, और अचानक आई बाढ़ में बह जाता है। इसके विपरीत, बुद्धिमान व्यक्ति का घर चट्टान पर बना होता है, और इसलिए तेज हवाओं और भयानक लहरों के आने पर भी वह नहीं गिरता है।
इसका क्या अभिप्राय है? यीशु समझाता है कि मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच का अन्तर यीशु के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। दोनों ही विषयों में, वह व्यक्ति यीशु की शिक्षाएँ सुनता है, ठीक जैसे हम आज इन आयतों को पढ़ते समय सुनते हैं। अतः मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच अन्तर प्रतिक्रिया देने में है। मूर्ख व्यक्ति यीशु के वचन सुनता है परन्तु उनके विषय में कुछ नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति यीशु के वचन सुनता है और उन्हें अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है, पश्चाताप करता है, और संसार को देखने और जीने के अपने पुराने तरीके से मुड़कर राज्य के तरीके की ओर आगे बढ़ता है। अपने पत्र में, याकूब यीशु के वचनों पर विचार करता है और मूर्ख का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो दर्पण में देखता है और फिर चला जाता है तथा तुरन्त भूल जाता है कि वह कैसा दिखता था (याकूब 1:23–24)। यह स्वयं को धोखा देना है (याकूब 1:22)। वहीं, बुद्धिमान व्यक्ति यीशु के वचन सुनता है और वही करता है जो वह कहता है। याकूब इस व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार करता है कि: “पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है।” यह व्यक्ति “धन्य होगा” और फलता-फूलता जाएगा (याकूब 1:25)। ध्यान दें कि इन दोनों घरों के बीच का अन्तर केवल बाहरी ओर से देखने से नहीं पहचाना जा सकता है। दोनों ही घर सुन्दर दिखाई देते हैं। परन्तु मुख्य अन्तर उनकी छिपी हुई नींव में है, या उसकी कमियों में है।
अतः 7:13-27 में मार्गदर्शन का सन्देश क्या है?
उपदेश का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से प्रेरित करना है कि व्यक्ति सिद्धता में बढ़ता चला जाए, और ऐसी धार्मिकता में बढ़े जो केवल बाहरी न होकर भीतर तक पहुँचती हो। इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, यीशु हमें तीन स्मरण रखने योग्य दृष्टान्त बताता है: अर्थात् चौड़ा और संकरा मार्ग, सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता, तथा बुद्धिमान और मूर्ख घर बनाने वाले। प्रत्येक विषय में बात एक ही है कि — केवल बाहरी दिखावट ही नहीं, वरन् आन्तरिक हृदय महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन पाया हुआ शिष्य वह होता है जो अधिक कठिन मार्ग, मन से, परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए यीशु के निमंत्रण को सुनता है। बाहरी व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है क्योंकि यह अधिक नियंत्रित और कम हस्तक्षेप करने वाला प्रतीत होता है। परन्तु यीशु स्पष्ट करता है कि यह वास्तव में बुद्धि नहीं है। यह तो विनाश की ओर ले जाने वाला चौड़ा मार्ग है। यह दिखावटी योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा स्वयं के प्रचार करने का तरीका है जो दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानता है। इसलिए यह तो मूर्ख लोगों का मार्ग है, जो उस घर के लिए दीवारें और छत बनाते हैं जो परीक्षाओं, कठिनाइयों और अन्तिम न्याय के समय भयानक रूप से ढह जाएगा। मार्गदर्शन प्राप्त शिष्य यीशु के इन वचनों को सुनता है और मूर्खता के मार्ग से हट जाता है ताकि वह आज भी और अनन्तकाल तक भी जीने योग्य जीवन प्राप्त कर सके।
चर्चा एवं मनन:
- आपके मन की कौन सी स्थिति ऐसी है जिसे यीशु की बुद्धिमानी के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है?
- आप ऐसा हृदय कैसे विकसित कर सकते हैं जो परमेश्वर और उसके राज्य की इच्छा रखता हो?
निष्कर्ष
यह समझना कठिन नहीं है कि क्यों यीशु का पहाड़ी उपदेश आज भी समस्त मसीही समझ और जीवन का केन्द्र बना हुआ है। यीशु के वचन स्मरणीय, आँखें खोलने वाले और चुनौतीपूर्ण हैं। वे एक ही साथ गहरे, व्यावहारिक, ईश्वर विज्ञान और पास्टरीय स्वभाव के हैं।
हम चाहे उसके तीखे सन्देश से बचने का कितना भी प्रयास करें, परन्तु जो कोई भी उपदेश को सच्चाई से पढ़ेगा, उसे अपने कष्ट तथा बिखरेपन और फरीसियों के समान जीवन जीने की प्रवृत्ति के विषय में अधिक जानकारी मिलेगी — जो अपने हृदय को देखने के विपरीत व्यवहार को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने से प्रसन्न होते थे।
वास्तव में, यीशु के सन्देश को अपने हृदय में ग्रहण करना कठिन है, भले ही उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें सिद्धता में बढ़ने वाली व्यक्तित्व की धार्मिकता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा हम स्वयं उसके आने वाले राज्य का हिस्सा नहीं बन पाएँगे, जीवन की ओर ले जाने वाले मार्ग पर नहीं होंगे, और वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होंगे जिसका घर न्याय के दिन भी टिका रह सके। यह कठिन इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक भक्ति करने वाले और परिपक्व लोग भी, यदि वे सच्चे हैं, फिर भी उनके मन में कामुकता, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, चिन्ता, पैसे के प्रति प्रेम, दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा और गलत उद्देश्य होने के कई क्षण आते हैं। जब हम अपने भीतर झाँककर देखते हैं कि हमारा हृदय हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि किसी का भी उद्धार नहीं होगा?
इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मत्ती रचित सुसमाचार को पूरी रीति से पढ़ने से मिलता है। हमें यह स्मरण कराया जाता है कि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए संसार में आया (1:21), और हमारे स्थान पर मृत्यु का सामना करके परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक नई वाचा स्थापित की, जो यीशु के प्रायश्चित बलिदान पर आधारित है (26:27–29)। यीशु निरन्तर हम पर करुणा की दृष्टि से देखता है (9:36)। परमेश्वर हमारा पिता है और हमें आनन्द के साथ देता है। हमें केवल माँगना है (7:7-11)। और हम 11:28 में यीशु के सामर्थी वचनों पर लौटते हैं, “हे सब परिश्रम करनेवालो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।”
जब भी हम कोई कौशल सीख रहे होते हैं — जैसे कि गाड़ी चलाना, गोल्फ खेलना, भाषा सीखना आदि — तो हम ठोकर खाते हैं, गलती करते हैं और संघर्ष करते हैं। उसी प्रकार यीशु का अनुसरण करना भी होता है। यीशु के आरम्भिक शिष्य और पिछले 2000 वर्षों से प्रत्येक स्थान पर हर शिष्य ने ठोकर खाई है, संघर्ष किया है और अधिकतर असफल रहे हैं। सच्चा मार्गदर्शन ऐसा ही होता है। परमेश्वर की दया और भलाई को ध्यान में रखते हुए, हम निडर होकर और सिद्ध न होते भी यीशु के इस निमंत्रण को ग्रहण कर सकते हैं कि, “मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो; और मुझसे सीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ: और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे” (11:29)।
अन्तिम टिप्पणियाँ
- पहाड़ी उपदेश की अधिक विस्तृत व्याख्या के लिए देखें: जोनाथन टी. पेनिंगटन, द सर्मन ऑन द माउंट एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग: ए थियोलॉजिकल कमेंट्री (बेकर अकैडमिक, 2017)।
विषयसूची
- 1
- मत्ती रचित सुसमाचार शिष्य बनाने वाली पुस्तक के रूप में है
- प्रसिद्ध उपदेश पर ध्यान देना: पहाड़ी उपदेश
- चर्चा एवं मनन:
- 2
- आनन्द के विषय में हमारी धारणाओं को नया रूप देना (5:3–16)
- चर्चा एवं मनन
- 3
- दूसरे लोगों के साथ हमारे सम्बन्धों को लेकर परमेश्वर किस बात की चिन्ता करता है? (5:17–5:48)
- चर्चा एवं मनन:
- 4
- परमेश्वर हमारे और अपने सम्बन्ध में किस बात की चिन्ता करता है?(6:1–21)
- मनन के लिए प्रश्न
- 5
- संसार की वस्तुओं और लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध के विषय में परमेश्वर किस बात की चिन्ता करता है? (6:19–7:12)
- मनन के लिए प्रश्न
- 6
- यीशु का निष्कर्ष: भाग एक
- यीशु का निष्कर्ष: भाग दो
- यीशु का निष्कर्ष: भाग तीन
- चर्चा एवं मनन: